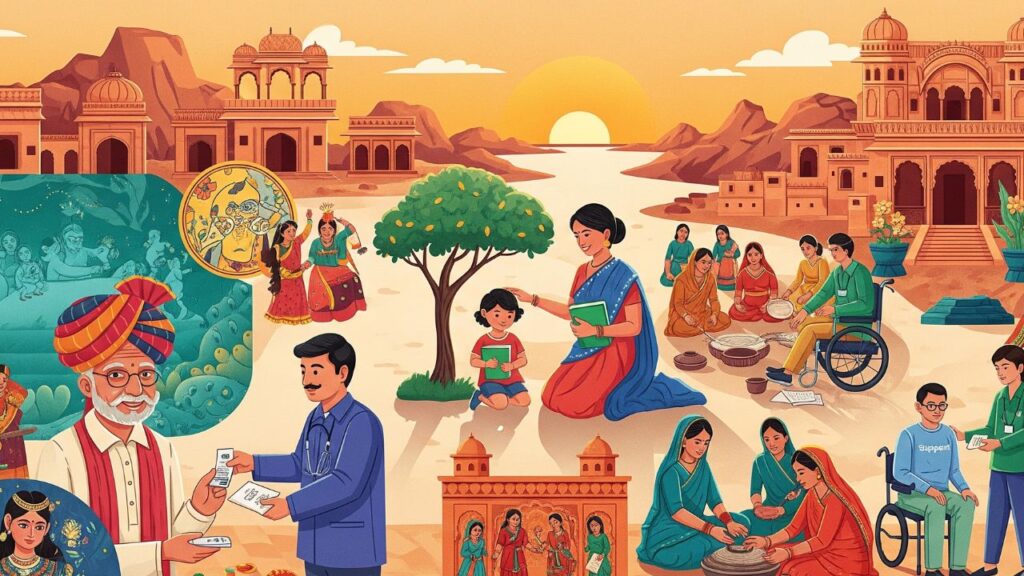राजस्थान में शिक्षा का भविष्य: भारत के सबसे बड़े राज्यों में से एक, राजस्थान अपनी ऐतिहासिक भव्यता और जीवंत संस्कृति के लिए जाना जाता है। इस गौरवशाली भूमि पर शिक्षा का भी गहरा महत्व रहा है। वर्तमान में, राज्य में स्कूली शिक्षा एक गतिशील परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित करना है। यह लेख राजस्थान में स्कूली शिक्षा के वर्तमान परिदृश्य, इसे आकार देने वाली प्रमुख पहलों, सामने आने वाली चुनौतियों और एक उज्जवल भविष्य की दिशा में आगे की राह पर विस्तृत प्रकाश डालता है। राज्य सरकार और विभिन्न हितधारक मिलकर यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि राजस्थान की भावी पीढ़ियां ज्ञान और कौशल से सशक्त हों, ताकि वे न केवल व्यक्तिगत सफलता प्राप्त कर सकें बल्कि राज्य और राष्ट्र के विकास में भी योगदान दे सकें।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और विकास
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से, राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। रियासतों के दौर में शिक्षा कुछ वर्गों तक सीमित थी, लेकिन स्वतंत्र भारत में इसे सार्वभौमिक बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। शुरुआती दौर में शिक्षा तक पहुंच बढ़ाना प्राथमिक चुनौती थी। दूर-दराज के क्षेत्रों में स्कूलों की स्थापना, शिक्षकों की नियुक्ति और बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया गया। धीरे-धीरे, शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) 2009 जैसे कानूनों ने सभी बच्चों के लिए शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया, जिससे नामांकन दरों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। शिक्षा का अधिकार राजस्थान में निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के बच्चों के लिए 25% आरक्षण प्रदान करता है, जिससे शिक्षा में समानता को बढ़ावा मिला है। राज्य ने कई योजनाएं जैसे मध्याह्न भोजन (Mid-day Meal) योजना, निशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण और छात्रवृत्ति कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों को स्कूल लाने और उन्हें बनाए रखने का प्रयास किया है। दशकों से, शिक्षा विभाग ने कई सुधार लागू किए हैं, जिनमें पाठ्यक्रम संशोधन, मूल्यांकन प्रणालियों में बदलाव और शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं। इन प्रयासों ने राजस्थान को शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है, बावजूद इसके कि राज्य को भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता रहा है। राजस्थान शिक्षा का अधिकार हेल्पलाइन और आरटीई राजस्थान आवेदन जैसे शब्द इस पहल की ऑनलाइन खोज में महत्वपूर्ण हैं।
- शिक्षा का अधिकार, राजस्थान (RTE Rajasthan) की आधिकारिक लिंक: http://rajeduboard.rajasthan.gov.in/RTEAct (यह माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की साइट पर अधिनियम की जानकारी देती है, RTE प्रवेश के लिए पोर्टल अलग है)
- RTE राजस्थान प्रवेश पोर्टल: https://rajpsp.nic.in/RTE/Home/RTEAct.aspx
- RTE राजस्थान संबंधित शीर्ष कीवर्ड: RTE राजस्थान एडमिशन, शिक्षा का अधिकार ऑनलाइन फॉर्म राजस्थान, राजस्थान आरटीई लॉटरी रिजल्ट, आरटीई राजस्थान स्कूल लिस्ट, निशुल्क शिक्षा राजस्थान, आरटीई एडमिशन डेट राजस्थान
वर्तमान परिदृश्य और प्रमुख पहलें (जुलाई 2025 तक)
जुलाई 2025 तक, राजस्थान में स्कूली शिक्षा का परिदृश्य विभिन्न नवाचारों और योजनाओं के साथ तेजी से विकसित हो रहा है। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के क्रियान्वयन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है, जिसके सकारात्मक परिणाम दिखने लगे हैं।
1. नामांकन में वृद्धि और पहुंच: राजस्थान के सरकारी स्कूलों में कुल नामांकन लगातार बढ़ रहा है। विभिन्न प्रवेशोत्सव कार्यक्रमों, जैसे “मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान” (जिसका दूसरा चरण 1 जुलाई से 24 जुलाई 2025 तक चल रहा है) और “प्रवेश उत्सव अभियान” के माध्यम से, शिक्षक घर-घर जाकर हाउसहोल्ड सर्वे कर रहे हैं। इसका उद्देश्य 3 से 18 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा से जोड़ना और ड्रॉपआउट बच्चों को वापस स्कूल लाना है। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश में तीन से 19 साल के बच्चों का शत-प्रतिशत ठहराव स्कूलों में हो, जिसके लिए शिक्षकों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। हालांकि, अभी भी कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में 100 से अधिक स्कूलों में 20 से कम विद्यार्थी नामांकित हैं, जिस पर विभाग विलय की संभावना पर विचार कर रहा है। इसके बावजूद, कुल मिलाकर सरकारी स्कूलों में अभिभावकों का विश्वास बढ़ा है, जिसके परिणामस्वरूप निजी स्कूलों की तुलना में सरकारी स्कूलों में अधिक छात्र पढ़ रहे हैं।
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 का क्रियान्वयन: NEP 2020 का क्रियान्वयन राजस्थान की शिक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण बदलाव ला रहा है। जुलाई 2025 से नए सत्र में कक्षा 1 से 6 तक की पुस्तकें नई शिक्षा नीति के तहत तैयार की गई हैं और उनका वितरण शुरू हो गया है। कक्षा 7 से 12वीं तक की पुस्तकों की छपाई भी चल रही है। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (RSCERT) द्वारा तैयार किया गया यह नया पाठ्यक्रम भारतीय इतिहास, संस्कृति, समकालीन उपलब्धियों और स्थानीय भाषाओं पर विशेष जोर देता है। नीति का मुख्य उद्देश्य रटने की प्रवृत्ति को कम कर रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच और सीखने की क्षमता को बढ़ावा देना है। शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात को 30:1 से कम रखने और सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों में इसे 25:1 करने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, छात्रों के नियमित स्वास्थ्य जांच और हेल्थ कार्ड जारी करने का प्रावधान भी NEP का हिस्सा है।
3. डिजिटल शिक्षा पहलें और एकीकृत पोर्टल: कोविड-19 महामारी के दौरान डिजिटल शिक्षा का महत्व उजागर हुआ, और राजस्थान ने इस दिशा में कई अग्रणी कदम उठाए हैं, जिनका विस्तार 2025 में भी जारी है:
- SMILE (Social Media Interface for Learning Engagement): WhatsApp के माध्यम से ई-लर्निंग सामग्री प्रदान करने का यह मंच अभी भी सक्रिय है, जिससे दूर-दराज के छात्रों तक शिक्षा पहुंच रही है।
- शिक्षा दर्शन और शिक्षा वाणी: ये शैक्षिक टीवी और रेडियो कार्यक्रम विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी एक चुनौती है।
- DIKSHA – RISE (Rajasthan Interface for School Educators): यह शिक्षकों के लिए डिजिटल प्रशिक्षण मॉड्यूल और ई-सामग्री प्रदान करता है, जिससे वे NEP के अनुरूप शिक्षण विधियों को अपना सकें। 2024 में 1 लाख से अधिक शिक्षकों को इस पर प्रशिक्षित किया गया।
- ई-कक्षा और मिशन ज्ञान: YouTube वीडियो और विभिन्न ऐप्स के माध्यम से छात्रों के लिए डिजिटल शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे सीखने को अधिक इंटरैक्टिव और आकर्षक बनाया जा सके।
- डिजिटल प्रवेशोत्सव: 1 जुलाई 2025 से शुरू हुए “मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान” के तहत डिजिटल प्रवेशोत्सव चलाया जा रहा है, जिसमें शिक्षक ऐप के जरिए बच्चों का दाखिला कर रहे हैं।
इन डिजिटल पहलों के केंद्र में शिक्षा पोर्टल राजस्थान और शाला दर्पण राजस्थान जैसे एकीकृत मंच हैं, जो प्रशासनिक दक्षता और शैक्षिक पहुंच दोनों को बढ़ाते हैं।
- शिक्षा पोर्टल, राजस्थान (Shiksha Portal Rajasthan): यह एक व्यापक डिजिटल पहल है जिसका उद्देश्य राजस्थान में शिक्षा से संबंधित सभी जानकारी और सेवाओं को एक ही मंच पर उपलब्ध कराना है। इसमें छात्रों के डेटा, शैक्षणिक सामग्री, मूल्यांकन रिपोर्ट और विभिन्न योजनाओं की जानकारी शामिल होती है। यह पोर्टल राजस्थान शिक्षा विभाग पोर्टल के रूप में भी जाना जाता है और शिक्षा से जुड़े विभिन्न हितधारकों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है।
- आधिकारिक लिंक: http://rajrmsa.nic.in/ (यह राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की मुख्य साइट है, जिस पर शिक्षा से संबंधित जानकारी उपलब्ध होती है। समग्र शिक्षा पोर्टल के विभिन्न मॉड्यूल इसी के अंतर्गत आते हैं।)
- संबंधित शीर्ष कीवर्ड: राजस्थान शिक्षा पोर्टल लॉगिन, शिक्षा विभाग राजस्थान, राजस्थान शिक्षा न्यूज, शिक्षा पोर्टल राजस्थान अपडेट्स, शिक्षा पोर्टल स्टूडेंट डिटेल्स
- शाला दर्पण, राजस्थान (Shala Darpan Rajasthan): यह राजस्थान सरकार का एक एकीकृत ऑनलाइन प्रबंधन पोर्टल है जो राज्य के सभी सरकारी स्कूलों, छात्रों और शिक्षकों से संबंधित जानकारी को प्रबंधित करता है। यह स्कूलों के प्रदर्शन की निगरानी, छात्रों की प्रगति पर नज़र रखने और शिक्षकों के डेटा को अपडेट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शाला दर्पण स्टाफ कॉर्नर, शाला दर्पण स्टूडेंट डिटेल्स, शाला दर्पण स्कूल लॉगिन और शाला दर्पण रिजल्ट इसके प्रमुख कार्य हैं। यह शाला दर्पण राजस्थान पोर्टल शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और दक्षता लाता है।
- आधिकारिक लिंक: https://rajshaladarpan.nic.in/
- संबंधित शीर्ष कीवर्ड: शाला दर्पण लॉगिन, शाला दर्पण स्टाफ कॉर्नर, शाला दर्पण स्कूल जानकारी, राजस्थान शाला दर्पण पोर्टल, शाला दर्पण शिक्षक आईडी, शाला दर्पण रिजल्ट, शाला दर्पण अवकाश आवेदन
4. बुनियादी ढांचे का विकास और सुरक्षा: राज्य सरकार स्कूलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में “आदर्श” (वरिष्ठ माध्यमिक) और “उत्कृष्ट” (प्राथमिक) विद्यालयों को उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। नए क्लासरूम का निर्माण, विज्ञान लैब, पुस्तकालय और शौचालय जैसी सुविधाओं का उन्नयन लगातार जारी है। बजट 2025-26 में विद्यालयों में क्लासरूम, लैब, कंप्यूटर लैब और शौचालयों के निर्माण पर ₹225 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है, साथ ही 15 हजार विद्यालयों में CCTV कैमरे लगाने और 1500 विद्यालयों में अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की भी योजना है।
हालांकि, हाल ही में झालावाड़ में स्कूल की छत गिरने जैसी दुखद घटनाओं ने स्कूल भवनों की सुरक्षा के मुद्दे को गंभीर रूप से उजागर किया है। जुलाई 2025 में हुई इस घटना के बाद, केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए व्यापक उपाय करने और सभी स्कूलों में अनिवार्य सुरक्षा ऑडिट कराने का निर्देश दिया है। राजस्थान में भी 8000 सरकारी स्कूल जर्जर हालत में पाए गए हैं, जिनमें से केवल 2000 स्कूलों की मरम्मत के लिए ₹175 करोड़ का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है, जिसकी राशि अभी तक नहीं मिली है। यह मुद्दा तत्काल ध्यान और ठोस कार्रवाई की मांग करता है।
5. शिक्षक सशक्तिकरण और भर्ती: शिक्षा की गुणवत्ता में शिक्षकों की भूमिका सर्वोपरि है। राजस्थान सरकार शिक्षकों के व्यावसायिक विकास और क्षमता निर्माण पर लगातार ध्यान दे रही है। NEP-अनुकूल शिक्षाशास्त्र पर प्रशिक्षण, डिजिटल उपकरणों का उपयोग और अनुभवात्मक सीखने पर जोर दिया जा रहा है। शिक्षकों के लिए नियमित कार्यशालाएं और सेमिनार आयोजित किए जाते हैं।
शिक्षक रिक्तियों को भरना एक महत्वपूर्ण चुनौती रही है। जुलाई 2025 में, RPSC द्वारा फर्स्ट ग्रेड शिक्षक के 3,225 पदों और माध्यमिक शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अध्यापक के 6,500 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की गई है। इसके अतिरिक्त, शारीरिक शिक्षा शिक्षकों (PTI) के 2000 पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इन भर्तियों से शिक्षकों की कमी को काफी हद तक पूरा करने में मदद मिलेगी।
6. समावेशी शिक्षा और लैंगिक समानता: राजस्थान समावेशी शिक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है, यह सुनिश्चित करते हुए कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) को मुख्यधारा की शिक्षा प्रणाली में एकीकृत किया जाए। उनके लिए विशेष शिक्षक, ब्रेल पुस्तकें, सहायक उपकरण और सुलभ क्लासरूम की व्यवस्था की जा रही है।
लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी कई योजनाएं चल रही हैं। “मुख्यमंत्री लाडो प्रोत्साहन योजना 2025” एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत बेटियों के जन्म से लेकर उनकी शिक्षा पूरी होने तक ₹2 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता (विभिन्न किस्तों में) प्रदान की जा रही है। यह योजना 1 अगस्त 2024 को शुरू हुई थी और बेटियों को जन्म पर ₹5,000, कक्षा 1, 6, 9, 10, 11, 12 में प्रवेश पर विभिन्न राशियां और 21 वर्ष की आयु पर शेष राशि प्रदान करती है। निःशुल्क साइकिल वितरण, परिवहन वाउचर और कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना जैसी पहलें भी लड़कियों को स्कूल तक लाने और उन्हें बनाए रखने में सहायक सिद्ध हुई हैं।
7. व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास: राष्ट्रीय शिक्षा नीति व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण पर जोर देती है, और राजस्थान इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। 500 से अधिक स्कूलों में कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, जो छात्रों को विभिन्न व्यवसायों के लिए तैयार करते हैं। बजट 2025-26 में कोटा में विश्वकर्मा कौशल संस्थान की स्थापना और 36 ITI के आधुनिकीकरण का लक्ष्य रखा गया है। प्रत्येक संभाग में ‘सेंटर फॉर एडवांस्ड स्किलिंग एंड करियर काउंसलिंग’ की स्थापना से छात्रों को करियर-उन्मुख कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी। दौसा जिले में 24 स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए व्यावसायिक शिक्षा योजना के तहत कौशल से जुड़े कोर्स (जैसे ऑटोमोबाइल, प्लंबर) शुरू किए गए हैं, जिनके लिए व्यावसायिक प्रशिक्षक (Vocational Trainers) लगाए जा रहे हैं।
प्रमुख चुनौतियां और गहन विश्लेषण:
राजस्थान में स्कूली शिक्षा में महत्वपूर्ण प्रगति के बावजूद, कई चुनौतियां बनी हुई हैं जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है:
1. स्कूल भवनों की सुरक्षा और गुणवत्ता: झालावाड़ में हालिया दुखद घटना (जुलाई 2025) ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठा दिया है। 8000 से अधिक सरकारी स्कूल भवनों का जर्जर होना और हजारों स्कूलों का लकड़ी के बल्लियों के सहारे टिके होना एक गंभीर चिंता का विषय है। यद्यपि मरम्मत के प्रस्ताव भेजे गए हैं, लेकिन फंड की कमी और धीमी प्रक्रिया बच्चों के जीवन को खतरे में डाल रही है। एक व्यापक, चरणबद्ध सुरक्षा ऑडिट और प्राथमिकता के आधार पर जीर्ण-शीर्ण भवनों की मरम्मत या पुनर्निर्माण के लिए पर्याप्त बजटीय आवंटन अनिवार्य है। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच समन्वित प्रयास की आवश्यकता है।
2. शिक्षक रिक्तियां और गुणवत्ता: यद्यपि नई भर्तियां जारी हैं, फिर भी दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में योग्य शिक्षकों की कमी एक बड़ी चुनौती है। विशेष विषयों जैसे विज्ञान, गणित और अंग्रेजी में शिक्षकों की उपलब्धता कम है। इसके अलावा, मौजूदा शिक्षकों के लिए निरंतर व्यावसायिक विकास (CPD) और आधुनिक शिक्षण पद्धतियों में प्रशिक्षण सुनिश्चित करना आवश्यक है ताकि वे NEP के लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त कर सकें। शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात को बनाए रखना भी एक सतत चुनौती है, खासकर कम नामांकन वाले स्कूलों में।
3. डिजिटल डिवाइड को पाटना: डिजिटल शिक्षा पहलें सराहनीय हैं, लेकिन शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच “डिजिटल डिवाइड” एक महत्वपूर्ण बाधा बना हुआ है। कई ग्रामीण परिवारों के पास स्मार्टफोन या इंटरनेट तक पहुंच नहीं है, जिससे वे इन ऑनलाइन संसाधनों का लाभ नहीं उठा पाते। बिजली की अनियमित आपूर्ति और कमजोर नेटवर्क भी इस समस्या को बढ़ाते हैं। इस खाई को पाटने के लिए स्कूलों में बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी, कंप्यूटर लैब और डिजिटल उपकरणों की उपलब्धता बढ़ाना आवश्यक है।
4. सीखने के परिणामों में सुधार: केवल नामांकन बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं है; वास्तविक चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करें और अपेक्षित सीखने के परिणाम हासिल करें। कई सरकारी स्कूलों में बच्चों के सीखने के स्तर अभी भी औसत से नीचे हैं। इसके लिए मूल्यांकन प्रणालियों में सुधार, उपचारात्मक शिक्षण (Remedial Teaching) और व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता है, खासकर उन छात्रों के लिए जो सीखने में पिछड़ रहे हैं।
5. लैंगिक असमानता और ड्रॉपआउट दर: लाडो प्रोत्साहन योजना जैसी पहलें लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा दे रही हैं, लेकिन ग्रामीण और सामाजिक रूप से रूढ़िवादी क्षेत्रों में अभी भी लैंगिक असमानता बनी हुई है। बाल विवाह, घरेलू जिम्मेदारियां और सुरक्षा संबंधी चिंताएं लड़कियों के बीच ड्रॉपआउट का कारण बनती हैं। यह सुनिश्चित करना कि लड़कियां माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर तक अपनी शिक्षा जारी रखें, एक सतत चुनौती है।
6. सामुदायिक और अभिभावक भागीदारी: स्कूल प्रबंधन समितियों (SMCs) को सशक्त बनाना और अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। कई बार अभिभावक अपनी भूमिका और बच्चों की शिक्षा में अपने योगदान के महत्व से अनभिज्ञ होते हैं। जागरूकता अभियान और नियमित माता-पिता-शिक्षक बैठकों के माध्यम से इसे मजबूत किया जा सकता है।
7. व्यावसायिक शिक्षा का विस्तार और स्वीकार्यता: यद्यपि व्यावसायिक शिक्षा का विस्तार हो रहा है, समाज में इसकी स्वीकार्यता अभी भी एक चुनौती है। छात्रों और अभिभावकों में पारंपरिक अकादमिक धाराओं के प्रति अधिक झुकाव देखा जाता है। व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा में लाने और इसे आकर्षक करियर विकल्प के रूप में प्रस्तुत करने के लिए जागरूकता और उद्योग-आधारित प्रशिक्षण पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।
भविष्य की दिशा और सिफारिशें:
राजस्थान में स्कूली शिक्षा को एक मजबूत और प्रगतिशील प्रणाली में बदलने के लिए निम्नलिखित दिशाओं और सिफारिशों पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है:
- बुनियादी ढांचे की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता: झालावाड़ जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए, राज्य के सभी स्कूल भवनों का तत्काल, व्यापक और अनिवार्य सुरक्षा ऑडिट किया जाना चाहिए। जर्जर भवनों की पहचान कर उनकी प्राथमिकता के आधार पर मरम्मत, सुदृढ़ीकरण या पुनर्निर्माण के लिए एक समयबद्ध योजना और पर्याप्त बजटीय आवंटन सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए केंद्र से विशेष सहायता भी मांगी जा सकती है।
- शिक्षक भर्ती और क्षमता निर्माण में तेजी: रिक्तियों को भरने के लिए पारदर्शी और त्वरित भर्ती प्रक्रियाएं अपनाई जाएं। विशेषकर ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षकों को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन पैकेज दिए जाएं। शिक्षकों के लिए NEP 2020 के अनुरूप निरंतर और गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम सुनिश्चित किए जाएं, जिसमें डिजिटल शिक्षण उपकरण, अनुभवात्मक शिक्षण और मूल्यांकन की नई पद्धतियां शामिल हों।
- डिजital शिक्षा का समतामूलक विस्तार: डिजिटल डिवाइड को पाटने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। स्कूलों में आवश्यक डिजिटल उपकरण और इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जाए। कमजोर वर्ग के छात्रों को उपकरणों तक पहुंच प्रदान करने के लिए योजनाएं शुरू की जा सकती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक डिजिटल सीखने के केंद्र स्थापित किए जा सकते हैं।
- सीखने के परिणामों पर केंद्रित दृष्टिकोण: केवल नामांकन ही नहीं, बल्कि बच्चों के वास्तविक सीखने के स्तर में सुधार पर जोर दिया जाए। नियमित और रचनात्मक मूल्यांकन प्रणालियां लागू की जाएं। प्रत्येक बच्चे की प्रगति पर नजर रखने के लिए डेटा-संचालित दृष्टिकोण अपनाया जाए और सीखने के अंतराल को पाटने के लिए उपचारात्मक शिक्षण पर अधिक ध्यान दिया जाए।
- प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ECCE) का सुदृढ़ीकरण: NEP के अनुसार, 3-8 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए मजबूत ECCE कार्यक्रम नींव का पत्थर हैं। आंगनवाड़ियों को स्कूलों के साथ बेहतर ढंग से जोड़ा जाए और उन्हें प्रशिक्षित शिक्षकों और पर्याप्त खेल-आधारित सीखने की सामग्री से लैस किया जाए।
- व्यावसायिक शिक्षा का मुख्यधारा में एकीकरण: व्यावसायिक शिक्षा को अधिक आकर्षक बनाने और उसे समाज में उचित सम्मान दिलाने के लिए पाठ्यक्रम को उद्योग की मांगों के अनुरूप बनाया जाए। छात्रों को इंटर्नशिप और ऑन-जॉब प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करने के लिए स्थानीय उद्योगों के साथ साझेदारी को बढ़ावा दिया जाए।
- सामुदायिक और अभिभावक भागीदारी को सशक्त बनाना: स्कूल प्रबंधन समितियों (SMCs) को अधिक सक्रिय और सशक्त बनाया जाए। अभिभावकों को बच्चों की शिक्षा में उनकी भूमिका के बारे में शिक्षित करने और उन्हें स्कूल की गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएं।
- स्वास्थ्य और पोषण पर निरंतर ध्यान: मध्याह्न भोजन योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। छात्रों के नियमित स्वास्थ्य जांच और मानसिक स्वास्थ्य सहायता सेवाओं को स्कूलों में उपलब्ध कराया जाए, जैसा कि झालावाड़ घटना के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने भी निर्देश दिया है।
- डेटा-संचालित नीति निर्माण: शिक्षा प्रणाली से संबंधित डेटा को नियमित रूप से एकत्र, विश्लेषण और उपयोग किया जाए ताकि नीतियों और कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से डिजाइन और संशोधित किया जा सके।
राजस्थान में स्कूली शिक्षा एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ी है। NEP 2020 के क्रियान्वयन और विभिन्न डिजिटल व विकासात्मक पहलों के साथ, राज्य एक समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रणाली की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। शिक्षा पोर्टल और शाला दर्पण जैसे डिजिटल मंच इस यात्रा में महत्वपूर्ण सहायक सिद्ध हो रहे हैं, जो पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करते हैं। हालांकि, स्कूल भवनों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, शिक्षकों की कमी को पूरा करना, डिजिटल असमानता को पाटना और सीखने के परिणामों को बेहतर बनाना अभी भी प्रमुख चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए सरकार, समुदाय, अभिभावकों और शिक्षकों के बीच एक समन्वित और सहयोगात्मक दृष्टिकोण आवश्यक है। यदि इन चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान किया जाता है, तो राजस्थान अपने युवाओं के लिए एक उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करने में सक्षम होगा, जिससे वे एक ज्ञान-आधारित समाज और अर्थव्यवस्था के निर्माण में सक्रिय भागीदार बन सकें।